Discussion: नई दिल्ली। आजादी के बाद से ही भारत में जातीय जनगणना की मांग उठती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह मांग तेज हो गई है। खासतौर पर विपक्षी दलों द्वारा केंद्र सरकार से पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की अपील की जा रही है। इन दलों का तर्क है कि “जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी” के सिद्धांत के तहत योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन होना चाहिए।
बिहार और तेलंगाना ने की जातीय गणना
जातीय जनगणना की इस मांग को तब और बल मिला जब बिहार सरकार ने 2023 में राज्य में जातीय गणना पूरी कर ली। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने भी राज्य में जातीय जनगणना कराकर आंकड़े सार्वजनिक कर दिए।
गौरतलब है कि भारत में आखिरी बार जातीय जनगणना 1931 में ब्रिटिश सरकार के दौरान हुई थी। इसके बाद 2011 की जनगणना में सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC) तो हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए।
2024 के लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना प्रमुख मुद्दा
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ का प्रमुख मुद्दा था। इस गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। हालांकि, चुनाव में हार के बावजूद यह मुद्दा अभी भी चर्चा में बना हुआ है।
जातीय जनगणना पर विरोध और समर्थन
जातीय जनगणना के समर्थन और विरोध में कई तर्क दिए जा रहे हैं:
✅ समर्थन करने वालों के तर्क:
- सामाजिक-आर्थिक असमानता को मापने का एक सटीक तरीका।
- आरक्षण और सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।
- पिछड़े वर्गों और वंचित समुदायों की सही पहचान हो सकेगी।
❌ विरोध करने वालों के तर्क:
- जातिगत जनगणना से समाज में विभाजन और फूट पैदा होगी।
- आर्थिक असमानता पर ध्यान देने की जरूरत है, न कि जातीय आंकड़ों पर।
- इससे सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंच सकता है।
बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का बयान
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जातीय जनगणना का विरोध करते हुए कहा कि “यह देश को बांटने वाला विषय है।” उन्होंने सुझाव दिया कि इसके बजाय अमीर-गरीब की गणना होनी चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकें।
उन्होंने कहा, “जनगणना का मकसद यह देखना होना चाहिए कि देश में कितने अस्पताल, स्कूल और पुलिस थाने की जरूरत है, न कि जातियों को गिनना।”
सरदार वल्लभभाई पटेल भी थे जातीय जनगणना के विरोध में
आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना के दौरान भी जातीय जनगणना की मांग उठी थी, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इससे देश की सामाजिक एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
जातीय जनगणना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- 1872-1931: ब्रिटिश सरकार ने हर जनगणना में जातिगत आंकड़े दर्ज किए।
- 1931: भारत में आखिरी बार जातीय जनगणना हुई, जिसमें 4,147 जातियों की पहचान की गई।
- 1941: जातीय जनगणना तो हुई, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए।
- 1951 के बाद: अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अलावा अन्य जातियों का डेटा प्रकाशित नहीं किया गया।
जातीय जनगणना क्यों जरूरी?
जातीय जनगणना की मांग करने वालों के अनुसार, इसके कई फायदे हो सकते हैं:
1️⃣ सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन – इससे पता चलेगा कि कौन-सी जाति किन हालातों में रह रही है।
2️⃣ आरक्षण की सही गणना – पिछड़े वर्गों को उनका सही प्रतिनिधित्व मिल सकेगा।
3️⃣ सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन – नीतियों को जातीय आंकड़ों के आधार पर और अधिक कारगर बनाया जा सकेगा।
जातिगत जनगणना: भविष्य की राह
जातिगत जनगणना एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक दोनों पहलू जुड़े हुए हैं। सरकार को यह तय करना होगा कि क्या यह जनगणना सामाजिक समानता लाने में सहायक होगी या समाज को विभाजित करने का कारण बनेगी।
साभार…














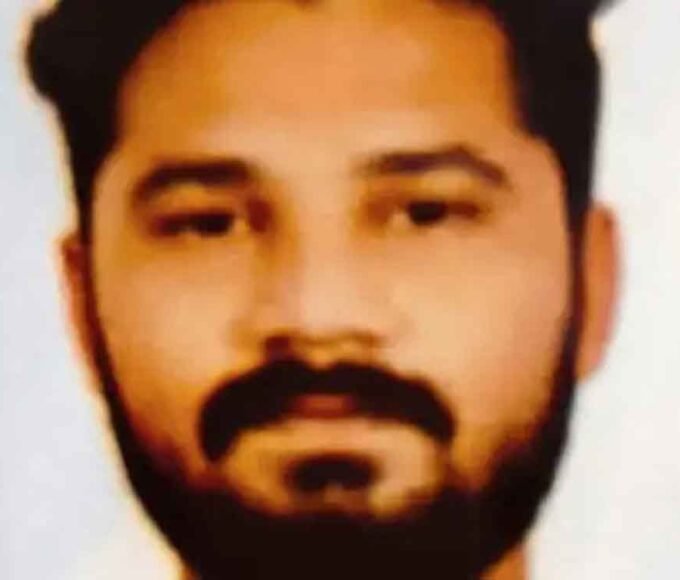

Leave a comment